हिंदी विरोधी छद्म नारों की राजनीति
Total Views | 14
_202503171506293390_H@@IGHT_400_W@@IDTH_800.jpg)
तमिलनाडु में भाषाई राजनीति को फिर से हवा दी जा रही है। चुनाव आते ही वहां के स्थानीय दल भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आजकल हिंदी उपनिवेशवाद का छइ नारा लगा रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पांच साल होने के बाद अब जाकर उन्हें इसकी याद आई है। स्टालिन को यह समझना होगा कि इस तरह की राजनीति से भले ही उन्हें क्षणिक लाभ हो जाए, परंतु उनका भाषाई विरोध राष्ट्रहित में नहीं है
वर्ष तमिलनाडु में विधानसभा अगले चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की आहट से ही वहां के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता एम. के. स्टालिन को हिंदी की याद आ आई। उन्हें लगने लगा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का षड्यंत्र कर रही है। दरअसल तमिलनाडु में जब भी कोई चुनाव आता है तो वहां के स्थानीय दलों को भाषा की याद सताने लगती है। उन्हें लगता है कि तमिल को नीचा दिखाकर हिंदी को उच्च स्थान पर स्थापित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। स्टालिन को पांच साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की याद आई। शिक्षा नीति के त्रिभाषा फार्मूले पर उन्हें आपत्ति है। उसके माध्यम से ही वे तमिल पर हिंदी के वर्चस्व की राजनीति को देखते हैं। यह एक राजनीतिक वातावरण बनाने की योजनावद्ध चाल है जिसमें तथ्य का अभाव है। 105 पृष्ठों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहीं भी हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं है। संभवतः शिक्षा नीति बनाने वालों को भारतीय भाषाओं की भावनाओं का ख्याल रहा होगा। संभव है कि वो तमिल राजनीति से आशंकित रहे होंगे। पता नहीं क्यों, स्टालिन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किस प्रविधान के तहत हिंदी थोपने का उपक्रम नजर आ गया है। जबकि पूरे दस्तावेज में कहीं हिंदी शब्द नहीं है। देखा जाए तो स्टालिन तमिलनाडु की जनता की संवेदनाओं को भड़काने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश की वे या तो हार गए या बाद में रूख बदलकर डीएमके के साथ हो गए। तमिलनाडु हिंदी उपनिवेशवाद को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में सवाल है कि कौन सा हिंदी उपनिवेशवाद और हिंदी थोपने की कौन सी कोशिश। स्टालिन इसे स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी विरोध के नाम पर कभी तमिल अस्मिता की बात करने लग जाते हैं तो कभी कुछ अन्य। संभव है कि उन्हें तमिलनाडु चुनाव में तात्कालिक लाभमिले, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर उनकी स्थिति हास्यास्पद हो रही है।
विगत दस वर्षों में तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रोन्नयन के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं। आज से करीब तीन वर्ष पहले काशी तमिल संगमम नाम से एक कार्यक्रम काशी में आरंभ किया गया था। इसका शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। यह कार्यक्रम तमिलनाडु और काशी के ऐतिहासिक संबंधों को फिर से याद करने और समृद्ध करने के लिए आयोजित किया गया था। तमिल को लेकर महाराष्ट्र और कश्मीर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे पूर्व 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिल के महान कवि सुब्रहृय भारती की सीवों पुण्यतिथि पर काशी हिंदी विश्वविद्यालय के कला विभाग में महाकवि के नाम पर सुब्रम्प भारती चेयर आन तमिल स्टडीज स्थापित करने की घोषणा की थी। ऐसे प्रकल्पों की लंबी सूची है। सिर्फ तमिल ही क्यों, ओडिया, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय बढ़ाने को लेकर भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस पूरे प्रसंग को देखने के बाद हिंदी के अप्रतिम लेखक कुबेरनाथ राय का एक निबंध 'जम्बुक' की कुछ पंक्तियों का स्मरण हो उठता है। कुबेरनाथ राय ने इस निबंध में बांग्ला के श्रेष्ठ साहित्यकार ताराशंकर बनर्जी की एक पंक्ति को उद्धृत किया है। उन्होंने लिखा है कि ताराशंकर बनर्जी ने बताया था कि बिना एक अखिल भारतीय जीवन दृष्टि विकसित किए हम अपना अस्तित्व बचा नहीं पाएंगे। यहां पर कुबेरनाथ जी आशंकित होते हुए लिखते हैं कि बनर्जी बात तो ठीक कर रहे हैं, परंतु क्षेत्रीय जीवन दृष्टि के बढ़ते जोर के सामने कोई अखिल भारतीय जीवन दर्शन की रचना करने में समर्थ हो सकेगा, इसमें संदेह है। क्रांतियुग में तिलक ने एक अखिल भारतीय जीवन दर्शन 'कर्मयोग' को सामने रखा था। इसके बाद महात्मा गांधी ने चरखा (स्वावलंबन और सर्वोदय हिंदी (राष्ट्रीय एकता) और अध्यात्म का त्रिकोणात्मक जीवन दर्शन सामने रखा। परंतु राजपट्ट बांधकर उनके शिष्य ही उसे अस्वीकृत कर गए। इसके बाद लोहिया ने एक अखिल भारतीय जीवन दृष्टि विकसित करने की चेष्टा की। परंतु न तो उनके पास है। पर्याप्त साधन थे और न ही कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी था जो उनके बोध को विकसित कर सके।
महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते थे। यह अकारण नहीं था कि उन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन में बड़े अभियानों का नाम हिंदी में रखा था। सविनय अवजा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, नमक सत्याग्रह आदि। लेकिन स्वाधीनता के बाद जब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन आरंभ हुआ, तब क्षेत्रीय जीवन दृष्टि को न केवल मजबूती मिली, बल्कि वो राजनीति के एक औजार की तरह भी विकसित होने लगा। भाषा विवाद के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने घुटने टेके थे, उस पर कुबेरनाथ राय को टिप्पणी गौर करने लायक है। एक तरफ वो मुट्ठी भर तमिल उपद्रवियों को कोसते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदी प्रातों के कुछ राजनीति-व्यवसायी या कुछ किताबी बुद्धीजीवी जो मौज से हर एक बात पर वाम बनाम दक्षिण की शैली में सोचते हैं।... 1947 से पूर्व आंख मूंदकर ऐसे ही प्रगतिशील पाकिस्तान का समर्थन करते थे (देखिए श्री राहुल की कहानी सुमेरपंडित) और फिर वैसे ही आंख मूंदकर सोचते हैं कि इस देश में वर्ग युद्ध तो संभव नहीं, अतः संप्रदाय युद्ध, जाति युद्ध, भाषा युद्ध कराओ जिससे बंसी लगाने का मौका मिल सके। कुबेरनाथ राय भाषा विवाद के समय देश के नेतृत्व पर बहुत कठोर टिप्पणी भी करते हैं और कहते हैं कि वर्तमान धृतराष्ट्र इस बार केवल अंधा ही नहीं, बल्कि बहरा भी है। कुबेरनाथ राय जब ऐसा कह रहे होंगे तो उनके मस्तिष्क में नेहरू रहे होंगे। ऐसा इस लेख के अन्य हिस्सों को पढ़कर प्रतीत होता दरअसल काफी लंबे समय से इस बात को कहा जाता रहा है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर रहा है।
वर्ष 1965 में अंग्रेजी पत्रिका 'क्वेस्ट' में अन्नदाशंकर राय की टिप्पणी है कि, भाषा संदर्भ में हिंदी का वही स्थान है जो राजनीतिक संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ का है। अतः धर्मनिरपेक्ष शासनतंत्र में दोनों के लिए कोई खास जगह नहीं है। उस टिप्पणी में अन्नदाशंकर राय के निष्कर्ष का आधार था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदी का प्रयोग करता है इस कारण हिंदी का संबंध हिंदू धर्म से है। विद्वान लोग भी कैसे भ्रमित होते हैं, यह उसका उदाहरण है । तभी तो कुबेरनाथ राय को उस लेख के प्रतिकार में लिखना पड़ा मुखौटा उतार लो, राय महाशय ! ऐसे में आज अगर स्टालिन तमिल को हिंदी के सामने खड़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं तो करें, पर यह न तो देश हित में है और न ही स्टालिन को राजनीति में किसी प्रकार से दीर्घकालीन लाभहोगा। संभव है कि हिंदी उपनिवेशवाद जैसे छद्म नारों के आधार पर वह कुछ सीटें जीत जाएं, लेकिन यह भी तय है कि उनकी राजनीति एक न एक दिन हारेगी। जब तक उन्हें यह समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वे तब तक तमिल का भी नुकसान कर चुके होंगे। यह समय भारतीय भाषाओं का स्वर्णकाल है, स्टालिन को समझना चाहिए।

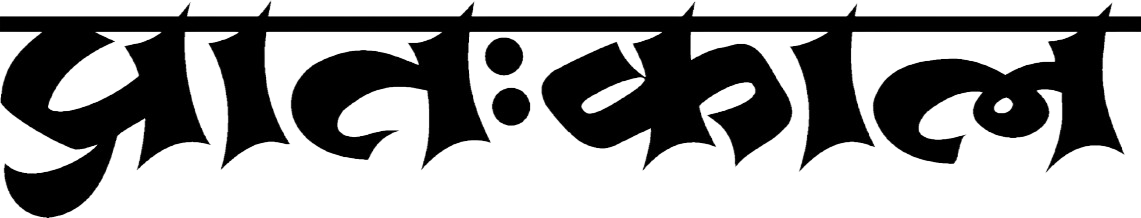


_202503211030463699.jpg)
_202503191451451533.jpg)

_202502071527150251.jpg)